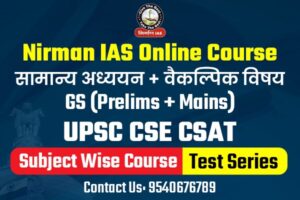विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का मामला
चर्चा में क्यों- समाचार एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) ने ANI के विकी पेज पर कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री की अनुमति देने के लिए विकिपीडिया के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।
UPSC पाठ्यक्रम:
प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ
मुख्य परीक्षा: GS-II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
मानहानि क्या है?
- मानहानि में किसी व्यक्ति के बारे में गलत बयान देना शामिल है जो उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है।
मानहानि को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है:
नागरिक मानहानि:
- किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए हर्जाना माँगना शामिल है।
- यह अपकृत्य कानून के अंतर्गत आता है।
आपराधिक मानहानि:
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत परिभाषित।
- इसमें किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाले झूठे बयान देना या प्रकाशित करना शामिल है, जिसके लिए दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
भारत में मानहानि के विरुद्ध कानून
भारत में मानहानि से निपटने के लिए मजबूत कानून हैं, जो प्रतिष्ठा को नुकसान से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
धारा 499 IPC:
- मानहानि को परिभाषित करती है और इसमें सत्य, सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक आचरण पर निष्पक्ष टिप्पणी जैसे अपवाद शामिल हैं।
- “जो कोई भी, बोले गए या पढ़े जाने वाले शब्दों द्वारा, या संकेतों या दृश्य चित्रणों द्वारा, किसी व्यक्ति के बारे में कोई आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना है, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा आरोप उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाएगा, तो, इसके बाद अपेक्षित मामलों को छोड़कर, उस व्यक्ति को बदनाम करने वाला कहा जाता है।”
धारा 500 IPC:
- मानहानि के लिए सजा निर्धारित करती है।
- “जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को बदनाम करता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।”
धारा 79:
- इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जैसे मध्यस्थों को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए देयता से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, बशर्ते वे कुछ शर्तों का पालन करें।
संशोधन और नियम:
- अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है, सबसे उल्लेखनीय रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008, और 2021 में मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की शुरूआत।
सिविल मानहानि:
इसमें सिविल कोर्ट में नुकसान के लिए मुकदमा दायर करना शामिल है, जहाँ यह साबित करने का भार दावेदार पर होता है कि बयान झूठा था और नुकसान पहुँचाया।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 क्या है?
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम) भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और डिजिटल लेनदेन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- यह डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सहित डिजिटल संचार के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है।
- अधिनियम का उद्देश्य सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा प्रदान करना और उपयोगकर्ताओं को साइबर अपराधों से बचाना है।
विकिपीडिया की भूमिका
- विकिपीडिया एक सहयोगी, ओपन-सोर्स, गैर-लाभकारी मंच के रूप में कार्य करता है।
- विकिपीडिया पर सामग्री दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाई और संपादित की जाती है, जिससे यह सामग्री निर्माता के बजाय एक मध्यस्थ बन जाता है।
- विकिपीडिया के खिलाफ ANI के मुकदमे का उद्देश्य मध्यस्थ को अपमानजनक सामग्री के लिए उत्तरदायी ठहराना है, यह एक कानूनी रणनीति है जो उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री को विनियमित करने की चुनौतियों को उजागर करती है।
‘सेफ हार्बर‘ क्लॉज
IT अधिनियम की धारा 79 के तहत सुरक्षित हार्बर क्लॉज मध्यस्थों को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए देयता से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बशर्ते कि वे:
- संचरण शुरू न करें।
- संचरण के रिसीवर का चयन न करें।
- सामग्री को संशोधित न करें।
इस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, मध्यस्थों को मध्यस्थ दिशा-निर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021 का पालन करना चाहिए, जो शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति को अनिवार्य करता है।
‘सेफ हार्बर‘ क्लॉज से जुड़ी चिंताएँ
हालाँकि, कई चिंताएँ हैं:
जिम्मेदारियों में अस्पष्टता: यह क्लॉज मध्यस्थ की जिम्मेदारियों की सीमा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है, जिससे विभिन्न व्याख्याएँ और असंगत प्रवर्तन होता है।
सामग्री मॉडरेशन चुनौतियाँ: मध्यस्थों को गैरकानूनी सामग्री को हटाने और मुक्त भाषण की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर अत्यधिक सेंसरशिप या अपर्याप्त मॉडरेशन होता है।
अनुपालन बोझ: मध्यस्थ दिशा-निर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021 के तहत आवश्यकताएँ, विशेष रूप से छोटे प्लेटफ़ॉर्म के लिए अनुपालन का एक महत्वपूर्ण बोझ जोड़ती हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और डेटा संरक्षण में प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण
सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008:
नए अपराधों की शुरूआत: साइबर आतंकवाद, पहचान की चोरी और बाल पोर्नोग्राफ़ी को विशिष्ट अपराधों के रूप में पेश किया गया।
डेटा सुरक्षा: डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को संबोधित करने के लिए धारा 43A और 72A पेश की गई, जिससे कंपनियों को डेटा उल्लंघन और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी बनाया गया।
मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021:
शिकायत निवारण तंत्र: मध्यस्थों को एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का आदेश देता है, जिसमें एक निवासी शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति शामिल है।
सामग्री विनियमन: गैरकानूनी सामग्री को हटाने और उपयोगकर्ता की शिकायतों को तुरंत संबोधित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आवश्यकताएँ लागू करता है।
पारदर्शिता: मध्यस्थों को समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।
संशोधनों के बावजूद, IT अधिनियम अभी भी कई गोपनीयता संबंधी चिंताएँ उठाता है:
डेटा संग्रह और उपयोग: धारा 43A और 72A डेटा सुरक्षा को संबोधित करते हैं, लेकिन इनका दायरा सीमित है, जिससे व्यापक डेटा गोपनीयता विनियमन में अंतराल रह जाता है।
निगरानी प्रावधान: अधिनियम धारा 69 के तहत व्यापक निगरानी शक्तियों की अनुमति देता है, जिससे राज्य के अतिक्रमण और व्यक्तिगत गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
उपयोगकर्ता नियंत्रण की कमी: उपयोगकर्ताओं के पास अक्सर अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण की कमी होती है, जिसमें सहमति और डेटा पोर्टेबिलिटी को प्रबंधित करने के लिए अपर्याप्त तंत्र होते हैं।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2023
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2023 का उद्देश्य डेटा गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित IT अधिनियम की कमियों को दूर करना है।
विधेयक की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
व्यापक डेटा सुरक्षा: व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक ढांचा स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि डेटा प्रसंस्करण निष्पक्ष, वैध और पारदर्शी हो।
उपयोगकर्ता अधिकार: उपयोगकर्ताओं को डेटा एक्सेस, सुधार, मिटाने और डेटा पोर्टेबिलिटी जैसे अधिकार प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिगत डेटा पर उपयोगकर्ता का नियंत्रण बढ़ता है।
डेटा सुरक्षा प्राधिकरण: अनुपालन की निगरानी, शिकायतों का समाधान और डेटा सुरक्षा विनियमों को लागू करने के लिए डेटा सुरक्षा प्राधिकरण (DPA) की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
क्रॉस-बॉर्डर डेटा ट्रांसफर: भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण के लिए शर्तें निर्धारित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता डेटा वैश्विक रूप से सुरक्षित है।