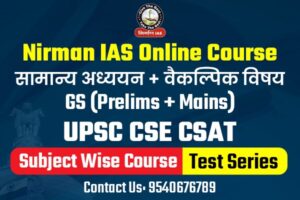|
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की सिफारिश: ‘सरकार मदरसों की फंडिंग बंद करे‘ |
चर्चा में क्यों-
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सिफारिश की है कि मदरसा बोर्ड को “बंद कर दिया जाए और मदरसों और मदरसा बोर्डों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला वित्त पोषण बंद कर दिया जाए और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को “औपचारिक स्कूलों” में दाखिला दिया जाए।
|
UPSC पाठ्यक्रम:
|
मदरसे क्या हैं और उन्हें कैसे वित्तपोषित किया जाता है?
- मदरसे पारंपरिक इस्लामी शैक्षणिक संस्थान हैं जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, अक्सर कुरान, हदीस और इस्लामी न्यायशास्त्र पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समय के साथ, कुछ मदरसों में धर्मनिरपेक्ष विषय भी शामिल किए गए हैं। भारत में, मदरसों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- मदरसा दरसे निज़ामी: ये मदरसे सार्वजनिक दान के रूप में संचालित होते हैं और राज्य के शैक्षिक पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- मदरसा दरसे आलिया: ये राज्य-स्तरीय मदरसा शिक्षा बोर्डों से संबद्ध हैं, जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का संयोजन प्रदान करते हैं।
वित्तपोषण स्रोत:
- सरकारी वित्त पोषण: मान्यता प्राप्त मदरसों को शिक्षकों के वेतन, बुनियादी ढांचे और अन्य शैक्षिक खर्चों के लिए राज्य सरकारों से वित्त पोषण मिलता है। उदाहरण के लिए, मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPQEM) पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाकर और वित्तीय सहायता प्रदान करके मदरसा शिक्षा में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार की पहल है।
- निजी और धर्मार्थ दान: गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को अक्सर निजी दान और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के धर्मार्थ संगठनों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।
मान्यता:
- मान्यता प्राप्त मदरसे मदरसा शिक्षा के लिए राज्य बोर्डों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड।
- गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे अक्सर लखनऊ में दारुल उलूम देवबंद या दारुल उलूम नदवतुल उलमा जैसे इस्लामी मदरसों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का पालन करते हैं।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी प्राथमिक भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ और कार्यक्रम भारत में बच्चों के संरक्षण और अधिकारों का पालन करें।
- NCPCR शिक्षा के अधिकार अधिनियम जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करके शिक्षा के अधिकार सहित बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में काम करता है।
- हाल ही में, NCPCR ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रखे जाने के बारे में चिंता जताई है और भारत में मदरसों के संचालन के तरीके में सुधार की सिफारिश की है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताएँ
- शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन: आयोग का दावा है कि मदरसों में पाठ्यक्रम RTE अधिनियम के अनुरूप नहीं है और इन संस्थानों में बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच से वंचित हैं।
- आपत्तिजनक सामग्री: रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कुछ मदरसे आपत्तिजनक सामग्री पढ़ाते हैं जो इस्लाम की सर्वोच्चता को बढ़ावा देती है, कुछ पाठ्यपुस्तकें पाकिस्तान में प्रकाशित की जाती हैं।
- योग्य शिक्षकों की कमी: रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मदरसों में अक्सर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की कमी होती है।
- धर्मनिरपेक्षता का पालन न करना: NCPCR का तर्क है कि मदरसे धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं और बच्चों को नियमित स्कूलों में दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित करते हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है?
- बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जिसे आमतौर पर शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के रूप में जाना जाता है, भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।
RTE अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा: अधिनियम में अनिवार्य किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि यह अधिकार पूरा हो।
- बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएँ: स्कूलों को कक्षाओं, स्वच्छता, शिक्षक-छात्र अनुपात और शिक्षण सामग्री से संबंधित कुछ मानकों को पूरा करना चाहिए।
- शिक्षक योग्यता: शिक्षकों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित योग्यताएँ पूरी करनी होंगी।
- समान पहुँच: यह अधिनियम प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिससे सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित होती है।
RTE अधिनियम पर 2024 का डेटा:
- शिक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, 2024 तक, भारत में 98% से अधिक बस्तियों में अब एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय तक पहुँच है, जो शिक्षा तक पहुँच में सुधार करने में RTE अधिनियम की सफलता को दर्शाता है।
- भारत में प्रारंभिक शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात (GER) 2024 में 96.7% तक पहुँच गया है, जो बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में लाने में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है।
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 29 और 30 भारतीय संविधान में संविधान के भाग III में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। ये अनुच्छेद सुनिश्चित करते हैं कि भारत में सभी वर्गों और समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और शैक्षिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।
अनुच्छेद 29:
अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक सुरक्षा
- यह अनुच्छेद भारत के किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है।
- इसमें प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग, भाषा या किसी विशेष क्षेत्र के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 29 (1): किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 29 (2): राज्य द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के समय केवल धर्म, जाति, लिंग, या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 30:
- अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार। यह अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रबंधित कर सकें।
मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 30 (1): सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 30 (2): राज्य सरकारें या केंद्र सरकार, अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती हैं, चाहे वह वित्तीय सहायता के संदर्भ में हो या किसी अन्य प्रकार से।
इन अनुच्छेदों का महत्व:
- ये अनुच्छेद भारत की सांस्कृतिक विविधता को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं।
- यह सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भेदभाव का सामना न करना पड़े।
- ये प्रावधान मदरसों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक समुदायों को उनके शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करने के लिए दिए गए अधिकारों के तहत संरक्षित किया जाता है।
भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा
- भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को एक मौलिक सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है, जहाँ राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, बिना किसी धर्म के पक्षपात या भेदभाव के।
भारतीय धर्मनिरपेक्षता:
- यह व्यक्तियों को धार्मिक संस्थाओं का अभ्यास करने, प्रचार करने और उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।
- यह यह भी सुनिश्चित करता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म न हो और कानून के समक्ष सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए।
पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अंतर:
- पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में, धर्म और राज्य के बीच का अंतर अधिक कठोर है।
- राज्य से अक्सर धार्मिक मामलों से खुद को पूरी तरह से अलग करने की अपेक्षा की जाती है, जबकि भारत में, धर्मनिरपेक्षता सभी समुदायों के बीच समानता और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए धर्मों के साथ सकारात्मक जुड़ाव की अनुमति देती है।
भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष चुनौतियाँ
1. शिक्षा की गुणवत्ता
- भारतीय शिक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक शिक्षा की गुणवत्ता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- कई स्कूलों में, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, प्रशिक्षित शिक्षकों, उचित बुनियादी ढाँचे और सीखने के संसाधनों की कमी है।
- वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 के अनुसार, कक्षा 5 में केवल 40% बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं, जो पूरे देश में खराब सीखने के परिणामों को दर्शाता है।
2. शिक्षकों की कमी
- भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है।
- शिक्षा मंत्रालय के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, कई राज्यों को शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कु
- छ सरकारी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:50 जितना अधिक है, जो निर्धारित मानदंडों से बहुत अधिक है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
3. ड्रॉपआउट दरें
- हाई ड्रॉपआउट दरें एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं, खास तौर पर माध्यमिक शिक्षा में।
- यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, माध्यमिक विद्यालय के लिए ड्रॉपआउट दर अभी भी लगभग 17.9% है, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, जो गरीबी, बाल श्रम और कम उम्र में विवाह जैसे सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण है।
4. बुनियादी ढांचे की कमी
- खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त स्कूल बुनियादी ढांचे से सीखने के माहौल में बाधा आती है।
- कई स्कूलों में उचित कक्षाएँ, शौचालय (खासकर लड़कियों के लिए), स्वच्छ पेयजल और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार, सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढाँचे में सुधार करना आवश्यक है, लेकिन कई क्षेत्रों में कार्यान्वयन धीमा है।
5. डिजिटल डिवाइड
- भारत में डिजिटल डिवाइड, जो COVID-19 महामारी के दौरान और अधिक स्पष्ट हो गया, ने शिक्षा में असमानताओं को बढ़ा दिया है।
- जबकि शहरी छात्रों के पास इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक बेहतर पहुँच है, ग्रामीण छात्र अक्सर सीमित या बिना पहुँच के संघर्ष करते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, केवल 32% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट तक पहुँच है, जिससे इन क्षेत्रों के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा संसाधनों तक पहुँचना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
6. शिक्षा तक असमान पहुँच
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जैसे हाशिए के समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और मध्याह्न भोजन योजना जैसी सरकारी पहलों के बावजूद, इन समूहों के लिए शैक्षिक प्राप्ति में अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर है, खासकर उच्च शिक्षा में।
7. नीतियों का खराब क्रियान्वयन
- हालाँकि भारत ने कई दूरदर्शी नीतियों को लागू किया है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, इन नीतियों का कार्यान्वयन कई क्षेत्रों में कमज़ोर बना हुआ है।
- उचित निगरानी का अभाव, अपर्याप्त धन और राजनीतिक हस्तक्षेप कुछ ऐसे कारक हैं जो इन सुधारों के सफल कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं।
भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल
1. समग्र शिक्षा अभियान (SSA)
- भारत में स्कूली शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए 2018 में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। यह योजना तीन पिछले कार्यक्रमों- सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) को एकीकृत करती है।
मुख्य विशेषताएँ:
- प्री-प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।
- बुनियादी ढाँचे, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा में सुधार पर जोर देता है।
- व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देता है और शिक्षा के विभिन्न स्तरों के बीच सहज संक्रमण सुनिश्चित करता है।
- 2024 में, सरकार ने इस योजना के लिए 38,800 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसमें स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और COVID-19 महामारी द्वारा बढ़ाए गए सीखने के अंतराल को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया गया।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 एक व्यापक रूपरेखा है जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। यह शिक्षा के लिए अधिक लचीला, समग्र और बहु-विषयक दृष्टिकोण बनाने पर केंद्रित है।
मुख्य विशेषताएं:
- नीति का लक्ष्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (GER) हासिल करना है।
- व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू की जाएगी, जिसमें अकादमिक शिक्षा के साथ व्यावहारिक कौशल को एकीकृत किया जाएगा।
- प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ECCE) पर जोर दिया गया है, जिसका लक्ष्य 2025 तक गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना है।
- बहुभाषावाद पर ध्यान केंद्रित करता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा देता है।
- ई-लर्निंग के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विकास सहित शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
3. मध्याह्न भोजन योजना (PM पोषण)
- मध्याह्न भोजन योजना, जिसका नाम बदलकर PM पोषण कर दिया गया है, बच्चों के स्कूल नामांकन, प्रतिधारण और पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सबसे सफल पहलों में से एक है। यह योजना पूरे भारत में सरकारी स्कूलों में छात्रों को मुफ़्त दोपहर का भोजन प्रदान करती है।
मुख्य विशेषताएँ:
- यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, जिससे स्कूलों में उपस्थिति और प्रतिधारण दर में सुधार हो।
- इस योजना से वर्तमान में देश भर में 11.8 करोड़ से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।
- 2024 के बजट में स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता और खाना पकाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है।
- इस योजना ने अधिक बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने और ड्रॉपआउट दरों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4. दीक्षा और स्वयं (डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म)
- शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, सरकार ने दीक्षा और स्वयं जैसी डिजिटल पहल शुरू की, जिससे छात्रों और शिक्षकों को शैक्षिक सामग्री तक मुफ़्त पहुँच मिली।
दीक्षा:
- एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो स्कूल-स्तरीय शिक्षण सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल और कई भाषाओं में आकलन प्रदान करता है।
- महामारी के दौरान यह एक मूल्यवान संसाधन बन गया है, जिसमें लाखों छात्र घर से ही शैक्षिक सामग्री प्राप्त कर रहे हैं।
स्वयं:
- एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) प्रदान करता है, जो स्कूल-स्तर से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा तक के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर मुफ़्त पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
- स्वयं शीर्ष संस्थानों से प्रमाणपत्र प्रदान करता है, जिससे उच्च शिक्षा अधिक सुलभ हो जाती है।
- इन प्लेटफ़ॉर्म ने भारत में डिजिटल शिक्षा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर COVID-19 महामारी के बाद।
5. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009
- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 एक ऐतिहासिक कानून है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।
मुख्य विशेषताएँ:
- यह अनिवार्य करता है कि इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है।
- कक्षाओं, स्वच्छता और शिक्षकों तक पहुँच जैसे बुनियादी ढाँचे के मानकों को सुनिश्चित करता है।
- जाति, लिंग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव या स्कूलों से निष्कासन को रोकता है।
- प्राथमिक शिक्षा में लगभग सार्वभौमिक नामांकन दर प्राप्त करने में RTE अधिनियम महत्वपूर्ण है।
- शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, 2024 में, भारत ने प्राथमिक स्तर पर 96.7% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त किया।
6. समग्र शिक्षा की डिजिटल पहल (NDEAR)
- 2021 में शुरू की गई राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR) का उद्देश्य स्कूलों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मानकीकृत और बेहतर बनाना है। यह प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा प्रणाली, यह सुनिश्चित करती है कि छात्रों और शिक्षकों के पास सर्वोत्तम डिजिटल संसाधनों तक पहुँच हो।
मुख्य विशेषताएँ
- छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और शिक्षा के शुरुआती चरणों से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है।
- ऑनलाइन शिक्षण, मूल्यांकन और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचे की तैनाती में स्कूलों का समर्थन करता है।
- 2024 में, NDEAR ने हाइब्रिड लर्निंग मॉडल का समर्थन करना जारी रखा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्र समान रूप से शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच सकते हैं।