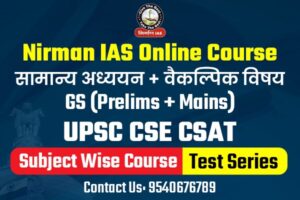|
धन शोधन निवारण अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय |
चर्चा में क्यों :-
- मनीष सिसोदिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी, अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र (त्वरित) सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया, तथा PMLA के तहत बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास में रखने की आलोचना की।
|
UPSC पाठ्यक्रम: प्रारंभिक परीक्षा: भारतीय राजनीति और शासन- संविधान, अधिकार मुद्दे मुख्य परीक्षा: GS-II: भारतीय राजनीति |
मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्य बातें
- मनीष सिसोदिया के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत शीघ्र (त्वरित) सुनवाई और जमानत प्रावधानों के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं।
- कोर्ट के फैसले के न केवल सिसोदिया बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी दूरगामी परिणाम हैं, जो बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास का सामना कर रहे हैं।
मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार की व्याख्या करते हुए इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार और त्वरित सुनवाई का अधिकार शामिल किया है।
- सिसोदिया के मामले में, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि देरी से चल रहे मुकदमों में इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, और अदालतों और अभियोजन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय तुरंत दिया जाए।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 का अनुप्रयोग
- निर्णय से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि त्वरित सुनवाई के अधिकार को PMLA की धारा 45 के अंतर्गत पढ़ा जाना चाहिए।
- आम तौर पर, धारा 45 जमानत देने पर कठोर शर्तें रखती है, जिसके लिए न्यायालय को संतुष्ट होना आवश्यक है कि:
- जमानत देने के लिए ट्रायल और संवैधानिक दोनों अदालतों को ‘ट्रिपल टेस्ट’ लागू करना आवश्यक है।
- ये तीन शर्तें हैं:
- (i) “यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि (आरोपी) ऐसे अपराध का दोषी नहीं है”
- (ii) “जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है”;
- (iii) आरोपी के भागने का जोखिम नहीं है।
- इन प्रतिबंधों के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास या धीमी सुनवाई प्रक्रिया जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती।
PMLA के तहत बेगुनाही साबित करने का बोझ
- PMLA के जमानत के प्रावधान सामान्य आपराधिक न्यायशास्त्र से अलग हैं, जहां दोष साबित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है।
- PMLA की धारा 45 के तहत, बेगुनाही साबित करने का बोझ अभियुक्त पर आ जाता है, जिससे उनके लिए जमानत प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
- इस कठोर उपाय के बावजूद, न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मुकदमे में प्रगति के बिना लंबे समय तक पूर्व-परीक्षण हिरासत में रहना जमानत देने को उचित ठहरा सकता है, भले ही सबूत का भार अभियुक्त पर ही क्यों न हो।
अनुच्छेद 21 क्या है?
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
- इसका उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा और गुणवत्ता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्याएँ:
मानव गरिमा का अधिकार:
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978): सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमापूर्ण अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए जीवन के अधिकार के दायरे का विस्तार किया।
निजता का अधिकार :
- के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017): सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल एक मौलिक अधिकार घोषित किया।
|
स्वास्थ्य का अधिकार:
- पी.बी. खेतारा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1993): न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है।
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार:
- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987): न्यायालय ने माना कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है।
मौलिक अधिकारों पर प्रभाव:
- अनुच्छेद 21 के विस्तार ने भारत में मौलिक अधिकारों के दायरे को काफी हद तक व्यापक बना दिया है, जिसमें मानवीय गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के विभिन्न पहलू शामिल हैं।
जमानत क्या है और इसके प्रकार
- जमानत एक कानूनी तंत्र है जिसके द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अस्थायी रूप से तब तक रिहा किया जाता है जब कि मुकदमा या अदालती कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती।
- जमानत यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति मुकदमे के दौरान भागने या कोई और अपराध किए बिना स्वतंत्र रह सकता है।
जमानत के प्रकार:
- नियमित जमानत: जब कोई व्यक्ति पुलिस या न्यायिक हिरासत में होता है तो दी जाती है।
- CRPC की धारा 437: जमानती और गैर-जमानती अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के लिए जमानत प्रावधानों से संबंधित है।
- CRPC की धारा 439: उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों को गैर-जमानती अपराधों के लिए जमानत देने का अधिकार है।
उदाहरण के लिए
- राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बनाम सीबीआई (2007) मामले में, अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नियमित जमानत दी थी।
अंतरिम जमानत:
- अग्रिम जमानत आवेदन लंबित रहने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी जमानत।
- उदाहरण के लिए, सुब्रत रॉय सहारा मामले में, व्यवसायी को उसकी नियमित जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय होने तक अंतरिम जमानत दी गई थी।
अग्रिम जमानत:
- जब कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से डरता है और हिरासत में लिए जाने से पहले जमानत मांगता है तो दी जाती है।
अग्रिम जमानत (धारा 438 CRPC)
प्रावधान:
- गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तारी की आशंका में व्यक्तियों को जमानत मांगने की अनुमति देता है।
- अनावश्यक हिरासत को रोकता है और गिरफ्तारी शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
न्यायिक शर्तें:
- अग्रिम जमानत देते समय न्यायालय अधिकार क्षेत्र को न छोड़ने, पासपोर्ट सरेंडर करने आदि जैसी शर्तें लगा सकते हैं।
उदाहरण के लिए
- अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कथित झूठे आरोपों के मामलों में उत्पीड़न को रोकने के लिए अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।
वैधानिक जमानत (धारा 436-A CRPC)
प्रावधान:
- उन विचाराधीन कैदियों को जमानत देता है जिन्होंने अपने ऊपर लगे अपराध के लिए अधिकतम सजा का आधा हिस्सा काट लिया है।
- इसका उद्देश्य जेलों में विचाराधीन कैदियों की आबादी को कम करना है।
- उपयोग:विशेष रूप से कम सजा वाले अपराधों के लिए आरोपित व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, यह सुनिश्चित करता है कि वे परीक्षण-पूर्व हिरासत में अत्यधिक समय न बिताएं।
क्या त्वरित सुनवाई से जेलों का भार कम होगा?
- एक त्वरित सुनवाई यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी व्यक्तियों को उचित समय के भीतर या तो दोषी ठहराया जाए या बरी किया जाए
- उदाहरण: हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) मामले में, यह पता चला कि हजारों विचाराधीन कैदी बिना किसी सुनवाई के वर्षों से जेलों में बंद थे।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने त्वरित सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई विचाराधीन कैदियों की रिहाई हुई और बिहार की जेलों में भीड़भाड़ कम हुई।
न्यायिक सुधार पहल:
- भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) की स्थापना ने मामलों के लंबित मामलों को हल करने में मदद की है, विशेष रूप से आपराधिक मामलों में, यह सुनिश्चित करते हुए कि परीक्षण अधिक तेज़ी से आगे बढ़ें, जिससे भीड़भाड़ वाली जेलों पर बोझ कम हो।
न्यायिक दक्षता:
- त्वरित परीक्षणों को लागू करने से न्यायपालिका में दक्षता को बढ़ावा मिलेगा, न्याय का तेज़ वितरण और संसाधनों का बेहतर आवंटन सुनिश्चित होगा।
भारत की न्यायपालिका के सामने से मुद्दे और चुनौतियां
न्यायिक देरी
- सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक लंबित मामलों की संख्या है। 2023 तक, भारतीय न्यायालयों में लाखों मामले लंबित हैं, जिससे न्याय प्रदान करने में काफी देरी हो रही है।
- उदाहरण: आरुषि तलवार हत्याकांड, जिसके निष्कर्ष पर पहुंचने में लगभग एक दशक लग गया, इस बात का उदाहरण है कि कैसे जांच में देरी,अपर्याप्त संसाधन और न्यायिक बैकलॉग के कारण मुकदमे लंबे समय तक चलते हैं।
अपर्याप्त बुनियादी ढांचा
- न्यायपालिका में अक्सर पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी होती है, जिसमें कोर्ट रूम की जगह से लेकर बुनियादी तकनीकी संसाधन शामिल हैं
- दिल्ली जिला न्यायालय परिसर अत्यधिक बोझ वाले न्यायालय कक्षों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से जूझ रहा है।
- उचित बुनियादी ढांचे और केस प्रबंधन प्रणालियों की कमी के कारण कई मामलों में देरी हुई है।
न्यायाधीशों की कमी
- 2023 तक, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्ति दर 30% के करीब थी।
- देश के सबसे बड़े न्यायालयों में से एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्वीकृत न्यायाधीशों की तुलना में कम न्यायाधीशों के साथ काम करता है, जिसके कारण 10 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की आलोचनाएँ
कठोर ज़मानत प्रावधान:
- PMLA धारा 45 की कठोर आवश्यकताओं के कारण अभियुक्त के लिए ज़मानत प्राप्त करना कठिन बनाता है, जहां निर्दोष साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। यह दोषी साबित होने तक निर्दोष के सिद्धांत के विरुद्ध है।
- उदाहरण: संजय राउत मामले (2022) में, PMLA की धारा 45 के प्रावधानों ने अभियुक्तों के लिए ज़मानत प्राप्त करना मुश्किल बना दिया। निर्णायक सबूतों के अभाव के बावजूद, ज़मानत की कड़ी शर्तों के कारण वह महीनों तक जेल में रहे।
जांच एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग:
- PMLA की आलोचना इस बात के लिए की गई है कि जांच एजेंसियों द्वारा राजनीतिक निशाना साधने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, कार्ति चिदंबरम मामले में, अभियुक्त ने दावा किया कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए कानून का दुरुपयोग किया गया, जिससे PMLA के मनमाने ढंग से लागू होने को लेकर चिंताएँ पैदा हुईं।
व्यापक परिभाषाएँ:
- भास्कर बनाम पटेल मामले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक परिभाषाएँ असंबंधित लेन-देन को PMLA के दायरे में ला सकती हैं, जिससे अभियुक्त व्यक्तियों के लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो जाता है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)
PMLA के मुख्य प्रावधान: धारा 3: मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को परिभाषित करती है। धारा 4: मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दंड निर्धारित करती है। धारा 19: अधिनियम के तहत गिरफ्तारी करने की शक्ति का विवरण देती है, जिसमें “विश्वास करने के कारण” दर्ज करने की आवश्यकता भी शामिल है। धारा 45: अधिनियम के तहत अभियुक्त को जमानत देने की शर्तें निर्धारित करती है। |