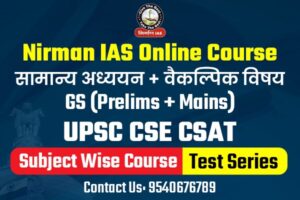भारत की एक्ट ईस्ट और इंडो-पैसिफिक नीतियों में थाईलैंड की भूमिका
UPSC पाठ्यक्रम:
प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ।
मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन II: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
चर्चा में क्यों:– हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा और वहां के प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा से मुलाकात के दौरान भारत-थाईलैंड संबंधों को “रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक उन्नत किया गया। यह कदम भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ और इंडो-पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पृष्ठभूमि
भारत और थाईलैंड के बीच संबंध केवल आधुनिक राजनीतिक या व्यापारिक नहीं हैं, बल्कि यह सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई आदान-प्रदान की सदियों पुरानी विरासत पर आधारित हैं।
धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंध
1. बौद्ध धर्म का सेतु
- भारत से बौद्ध धर्म की थेरवादा शाखा 3वीं शताब्दी ई.पू. में थाईलैंड पहुंची।
- आज भी थाईलैंड की 90% से अधिक आबादी थेरवादा बौद्ध धर्म का पालन करती है।
- थाई बौद्ध भिक्षु शिक्षा हेतु भारत के नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते रहे हैं।
2. रामायण से रामकियन तक
- भारत की रामकथा का थाई संस्करण “रामकियन” थाई कला, नृत्य, नाटक और साहित्य में व्यापक रूप से समाहित है।
- थाई किंग्स को राम (रामाथिबोदी) कहा जाता है और “राम” को थाई राजपरिवार में उच्च आदर्श माना गया है।
भाषाई और साहित्यिक प्रभाव
1. संस्कृत और पाली भाषा का प्रभाव
- थाई भाषा में संस्कृत और पाली से कई शब्द आए हैं, जैसे “धम्म” (धर्म), “राजा” (राजा), “सत्य”, आदि।
- थाई धार्मिक ग्रंथों और मंत्रों में पाली भाषा का आज भी उपयोग होता है।
2. शिक्षाव्यवस्था और धार्मिक अनुष्ठान
- थाईलैंड के बौद्ध मठों (वाट) में भारत से आए ग्रंथों और विचारधाराओं का उपयोग किया जाता है।
प्राचीन व्यापारिक संबंध
- दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार की ऐतिहासिक धारा रही है।
- चोल और श्रीविजय साम्राज्य के समय व्यापार, संस्कृति और धर्म का व्यापक आदान-प्रदान हुआ।
- भारत से मसाले, कपड़े, औषधियाँ थाईलैंड पहुंचती थीं, वहीं थाईलैंड से सुगंधित लकड़ियाँ और बहुमूल्य पत्थर भारत आते थे।
भारत-थाईलैंड सांस्कृतिक आदान-प्रदान की समकालीन रूपरेखा
- ICCR और MEA के माध्यम से दोनों देशों में सांस्कृतिक उत्सव, योग दिवस, और छात्रवृत्तियों का आयोजन होता है।
- भारत-थाईलैंड मैत्री संघ (India-Thai Friendship Association) सांस्कृतिक संपर्क को सशक्त बनाता है।
भारत की ‘Act East Policy’
भारत की ‘Act East Policy’ (पूर्व की ओर सक्रिय नीति) 2014 में ‘Look East Policy’ (पूर्व की ओर देखो नीति) के उन्नत संस्करण के रूप में प्रस्तुत की गई। इस नीति का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करना है।
1. ‘Look East Policy’ की उत्पत्ति
- 1991 में, भारत ने ‘Look East Policy’ की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करना था।
- यह नीति शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक परिदृश्य में बदलाव के संदर्भ में विकसित की गई थी।
2. ‘Act East Policy’ की आवश्यकता
2014 में, वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, ‘पूर्व की ओर देखो नीति’ को ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ में परिवर्तित किया गया। इसका उद्देश्य न केवल आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना था, बल्कि सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को भी सुदृढ़ करना था।
नीति के प्रमुख उद्देश्य
- आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना: आसियान (ASEAN) और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना।
- सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना: साझा सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क और समझ को बढ़ाना।
- रणनीतिक साझेदारी विकसित करना: क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास: भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ बेहतर संपर्क और विकास के अवसर प्रदान करना।
नीति के तहत प्रमुख पहल
कनेक्टिविटी परियोजनाएं:
- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग: यह राजमार्ग भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ता है, जिससे व्यापार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ता है।
- कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट: यह परियोजना म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह को मिजोरम से जोड़ती है, जिससे भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को समुद्री मार्ग से जोड़ा जा सकता है।
सांस्कृतिक सहयोग:
- नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण: भारत और पूर्वी एशियाई देशों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया गया है।
रणनीतिक साझेदारी:
- जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, और अन्य देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना।
इंडो-पैसिफिक रणनीति का महत्व
भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति का उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित क्षेत्र का समर्थन करना है। यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देता है, जिसमें सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाता है।
रणनीति के प्रमुख तत्व
1.मुक्त और खुला क्षेत्र:
- भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और खुलेपन का समर्थन करता है, जिससे सभी देशों को बिना किसी बाधा के नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता मिलती है।
2. समावेशिता:
- यह रणनीति सभी राष्ट्रों को शामिल करने पर बल देती है, जिससे कोई भी देश बाहर न रहे और सभी को समान अवसर मिले।
3.नियम-आधारित व्यवस्था:
-
अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना, जिससे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो और किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन न हो।
4. चीन की विस्तारवादी नीतियों के संदर्भ में
- भारत की यह रणनीति चीन की विस्तारवादी नीतियों के प्रति एक संतुलित प्रतिक्रिया है।
- चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों के मद्देनज़र, भारत एक विकासवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए क्षेत्रीय सहयोग और विकास पर जोर देता है।
- यह दृष्टिकोण ‘विकासवाद’ को ‘विस्तारवाद’ के विपरीत रखता है, जहां सहयोग और साझेदारी के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।
5. क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारियां
क्वाड (Quad):
- भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड समूह में सक्रिय भागीदारी करता है, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, खुलेपन और नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
आसियान (ASEAN):
- भारत आसियान की केंद्रीयता का समर्थन करता है और उनके साथ मिलकर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए कार्य करता है।
अन्य साझेदारियां:
- भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत कर रहा है, जिससे समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
हालिया घटनाक्रम
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा के दौरान भारत और थाईलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर पर उन्नत किया।
- इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने अपने सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक ‘रणनीतिक संवाद’ स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध, मानव तस्करी और अवैध प्रवास जैसे मुद्दों से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देना है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड सरकार का भारतीय साइबर अपराध पीड़ितों की वापसी में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि दोनों देशों की एजेंसियां मानव तस्करी और अवैध प्रवास के खिलाफ मिलकर कार्य करेंगी।
- यह सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
समझौते हस्ताक्षरित:
- डिजिटल तकनीक
- NMHC (लोटल, गुजरात)
- MSMEs
- उत्तर-पूर्व भारत-थाईलैंड सहयोग
- हस्तशिल्प
- समुद्री विरासत
BIMSTEC सम्मेलन:
- 6वां BIMSTEC शिखर सम्मेलन, समुद्री सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर।
- भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के नेताओं की उपस्थिति।
🔷 इस मुद्दे का महत्व
- रणनीतिक स्थिति: थाईलैंड की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संपर्क का सेतु है।
- आसियान में प्रवेश द्वार: थाईलैंड, भारत की ACT EAST नीति के तहत दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- उत्तर-पूर्व भारत का विकास: थाईलैंड के साथ व्यापार, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में सहायक।
- चीन की चुनौती का जवाब: एक स्वतंत्र और नियम-आधारित क्षेत्र को बढ़ावा देना, चीन की आक्रामकता के विरुद्ध सामरिक संतुलन स्थापित करता है।
🔷 आंकड़े व रिपोर्ट
- PIB (2025): भारत-थाईलैंड व्यापार 2023–24 में $17.7 बिलियन तक पहुंचा।
- NITI Aayog: उत्तर-पूर्वी भारत की विकास नीति में थाईलैंड के साथ संपर्क को प्राथमिकता दी गई है।
- ASEAN रिपोर्ट (2024): भारत, आसियान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- World Bank: BIMSTEC क्षेत्र में व्यापार लागत वैश्विक औसत से 30% अधिक है — संपर्क आवश्यक है।
🔷 सरकारी पहल
- एक्ट ईस्ट पॉलिसी डेस्क: विदेश मंत्रालय में पूर्वोत्तर भारत को ASEAN से जोड़ने हेतु विशेष डेस्क।
- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग: क्षेत्रीय संपर्क परियोजना, जो मणिपुर को थाईलैंड से जोड़ेगी।
- पीएम गति शक्ति योजना: उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को गति।
- बिम्सटेक तटीय नौवहन समझौता: समुद्री व्यापार की लागत कम करने की पहल।
🔷 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं
जापान: थाईलैंड के साथ साझा समुद्री गश्ती और तकनीकी सहयोग।
ऑस्ट्रेलिया: ‘प्रशांत स्टेप-अप’ रणनीति के अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ गहन जुड़ाव।
अमेरिका: हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF) के ज़रिए थाईलैंड के साथ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन।
🔷 संवैधानिक व नैतिक पहलू
- संविधान का अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देना।
- नैतिक दृष्टिकोण: विकासवाद बनाम विस्तारवाद — नैतिक विदेश नीति की अभिव्यक्ति।
- सांस्कृतिक कूटनीति: भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ रणनीति में रामायण, बौद्ध धर्म और योग जैसे तत्वों का नैतिक प्रभाव।
🔷 आगे की राह
- संरचनात्मक संपर्क: त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाए।
- सुरक्षा सहयोग: नियमित रणनीतिक संवाद, संयुक्त युद्धाभ्यास और खुफिया साझेदारी।
- MSME साझेदारी: MSME क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और मार्केट एक्सेस को बढ़ावा।
- नागरिक संपर्क: छात्रों, पर्यटकों और कलाकारों के लिए विशेष कार्यक्रम और वीज़ा सुविधा।
- बौद्ध सर्किट विस्तार: भारत-थाईलैंड संयुक्त बौद्ध पर्यटन पैकेज।